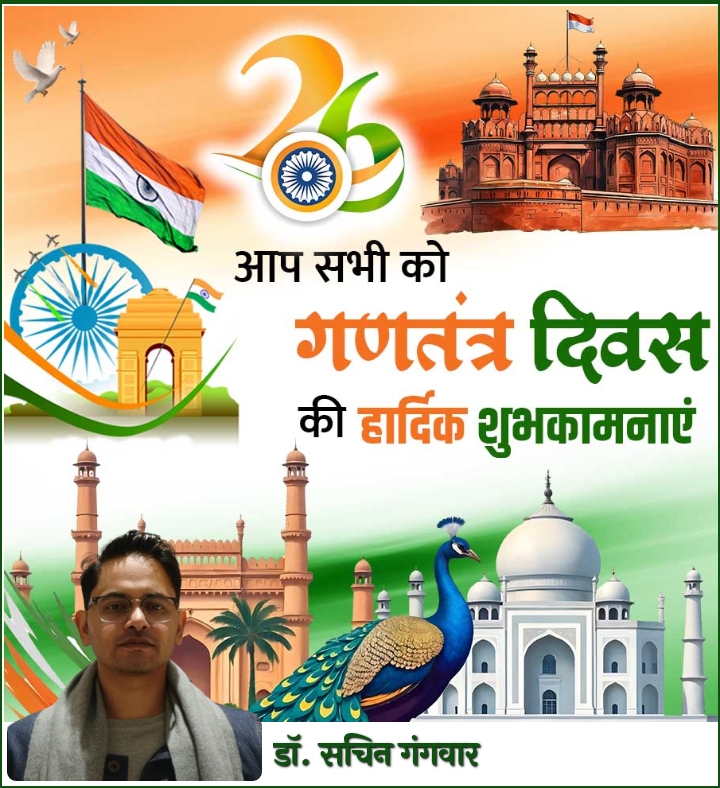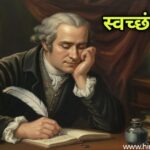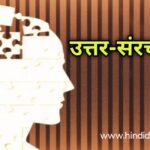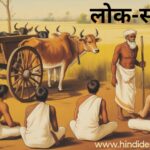प्रस्तावना
भारतीय काव्यशास्त्र में “रस” का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रस न केवल कविता या साहित्य का प्राण माना गया है, बल्कि यह एक दार्शनिक व कलात्मक अनुभूति का केंद्रबिंदु भी है। रस का मूल उद्देश्य है—साहित्यिक रचना के माध्यम से पाठक या श्रोता को भावानुभूति के चरम तक पहुँचाना। परंतु यह भावानुभूति कब, कैसे और किन तत्वों से उत्पन्न होती है—यही प्रश्न है “रस निष्पत्ति” (रस की उत्पत्ति) का।
रस निष्पत्ति की समस्या पर अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से विचार किया है और अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। यह लेख रस निष्पत्ति की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए विभिन्न आचार्यों की दृष्टियों को समेटता है और समग्र निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।
रस: एक परिचय
“रस” शब्द का मूल अर्थ है – ‘आनंद’, ‘स्वाद’ या ‘अनुभूति’। भरतमुनि ने “नाट्यशास्त्र” में रस को काव्य की आत्मा कहा है:
“रसात्मकम् वाक्यम् काव्यम्।”
(काव्य वह है जिसमें रस की अनुभूति होती है।)
भरत ने रस को आठ प्रकारों में वर्गीकृत किया—श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत। बाद में शांत रस को जोड़कर इनकी संख्या नौ हो गई।
रस निष्पत्ति का अर्थ
रस निष्पत्ति का तात्पर्य है—काव्य या नाट्य के तत्वों के मेल से जिस विशेष भावानुभूति या सौंदर्यानुभूति का उदय होता है, वह रस कैसे उत्पन्न होता है—इस प्रक्रिया को समझाना ही रस निष्पत्ति का उद्देश्य है।
यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है क्योंकि केवल भाव दिखा देने से रस की अनुभूति नहीं होती। रस तभी उत्पन्न होता है जब दर्शक/पाठक उसमें तन्मय होकर रसास्वादन करे। इस तन्मयता और आनंद की उत्पत्ति किन तत्वों से और कैसे होती है—यही रस निष्पत्ति की समस्या है।
भरतमुनि का दृष्टिकोण
भरत रस निष्पत्ति के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने कहा है:
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसं निपत्यते।”
(रस विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से उत्पन्न होता है।)
1. विभाव – रस का कारण है। ये दो प्रकार के होते हैं:
-
आलंबन विभाव – वह पात्र जिससे रस संबद्ध होता है (उदा. नायक-नायिका)
-
उद्दीपन विभाव – वे परिस्थितियाँ जो भाव को उद्दीप्त करती हैं (जैसे चंद्रमा, पुष्पवाटिका आदि)
2. अनुभाव – वह बाह्य क्रिया जो आंतरिक भाव को अभिव्यक्ति करती है (जैसे अश्रु, कंपन)
3. व्यभिचारी भाव – सहायक भाव, जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं (जैसे स्मृति, ग्लानि, उत्साह)
भरत ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि यह संयोग किसमें होता है—दर्शक में, पात्र में या नाटक में। अतः रस निष्पत्ति का प्रश्न उनके ग्रंथ में आरंभ तो हुआ, परंतु उसका समाधान आचार्य भामह, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त आदि ने आगे चलकर दिया।
भामह का दृष्टिकोण – अलंकारप्रधानता
भामह ने रस को काव्य का फल माना और उसका संबंध मुख्यतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों से जोड़ा। उनके अनुसार रस तब उत्पन्न होता है जब काव्य में उचित अलंकार और शैली हो। उन्होंने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को विश्लेषित नहीं किया, अतः उनका दृष्टिकोण अधूरा और सीमित है।
दंडी का दृष्टिकोण – दोषरहित भाषा और भावपूर्ण कथन
दंडी ने “काव्यादर्श” में कहा कि रस की निष्पत्ति तब होती है जब भाषा दोषरहित हो, भाव स्पष्ट हो और उसमें कलात्मकता हो। उन्होंने रस की उत्पत्ति को “अवस्था विशेष” कहा—यानी रस कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब पाठक/दर्शक काव्य के साथ तादात्म्य स्थापित कर ले।
वामन का दृष्टिकोण
वामन का मत है कि रस की निष्पत्ति तब होती है जब काव्य में औचित्य अर्थात् परिस्थिति, पात्र और प्रसंग के अनुसार भावों की उचित अभिव्यक्ति हो। उन्होंने कहा है:
“औचित्य ही काव्य का प्राण है”।
उनके अनुसार रस निष्पत्ति की कुंजी ‘औचित्य’ में निहित है—अनुचित स्थान पर भाव, विभाव या अनुभाव रखने से रस निष्पन्न नहीं होता।
आनंदवर्धन का दृष्टिकोण
आनंदवर्धन ने “ध्वन्यालोक” में रस को काव्य की आत्मा कहा। उन्होंने रस निष्पत्ति को “रसध्वनि” द्वारा व्याख्यायित किया। उनके अनुसार जब काव्य में रस अप्रत्यक्ष रूप से (व्यंजना शक्ति द्वारा) संप्रेषित होता है, तब रस निष्पन्न होता है।
“वाक्यार्थानुभवात् रसस्वादनम्”
अर्थात् रस तब उत्पन्न होता है जब पाठक वाक्य के सामान्य अर्थ से आगे जाकर उसके व्यंजित रस का अनुभव करता है।
मम्मट का दृष्टिकोण – सहृदयप्रधान निष्पत्ति
मम्मट ने “काव्यप्रकाश” में रस की निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा:
“रसो वा भावो रसानुभवो वा”
(रस स्वयं भाव नहीं बल्कि भाव की ऐसी अवस्था है जो सहृदय में अनुभव होती है।)
उनके अनुसार रस निष्पत्ति तभी संभव है जब:
-
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उपयुक्त हों
-
भाव स्थायी हों
-
सहृदय पाठक उसमें तन्मय हो
मम्मट ने रस को ‘रसस्वादन’ के रूप में सहृदय की चेतना में घटित होने वाला आनंद बताया।
अभिनवगुप्त का दृष्टिकोण
अभिनवगुप्त ने रस निष्पत्ति पर अत्यंत गहन दार्शनिक विवेचन किया। उनके अनुसार:
“रस न किसी पात्र में होता है, न काव्य में – वह सहृदय में होता है।”
उन्होंने “भावकतायोजन” की संकल्पना दी—कहने का तात्पर्य है कि पाठक/दर्शक जब अपने व्यक्तिगत अहं को भूलकर एक ‘भावक’ की भूमिका में आता है, तब रस की निष्पत्ति होती है।
अभिनवगुप्त के अनुसार रस निष्पत्ति की शर्तें:
-
भावकता – पाठक में तादात्म्य की योग्यता हो।
-
सामाजिक/सामूहिक स्मृति – सहृदय को विभाव, अनुभाव आदि की सांस्कृतिक पहचान हो।
-
अहं-निवृत्ति – पाठक अपनी व्यक्तिगत पीड़ा/सुख को भूलकर सार्वभौमिक स्तर पर अनुभव करे।
उदाहरणतः जब कोई करुण रस की कविता पढ़ता है, तो वह उसमें अपने जीवन का दुख नहीं खोजता, बल्कि एक सामान्य, सार्वभौमिक मानवीय पीड़ा को अनुभव करता है।
रस निष्पत्ति और सहृदय की भूमिका
सभी आचार्य इस बात पर सहमत हैं कि रस निष्पत्ति की अंतिम अवस्था पाठक/दर्शक के भीतर घटती है, और यह तभी संभव है जब वह ‘सहृदय’ हो—अर्थात् उसकी संवेदना प्रखर हो, वह काव्य में तादात्म्य स्थापित कर सके।
रस का अस्तित्व तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कोई सहृदय उसमें प्रवेश न करे। यह एक प्रकार की ‘रचनात्मक सहभागिता’ (creative participation) है, जहाँ पाठक भी रचना का सह-निर्माता बनता है।
रस निष्पत्ति: एक समन्वित दृष्टिकोण
विभिन्न आचार्यों की दृष्टियों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि रस निष्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित तत्त्वों की भूमिका होती है:
-
कविता का विषय (स्थायी भाव)
-
प्रस्तुतीकरण के उपकरण (विभाव, अनुभाव, संचारी भाव)
-
भाषिक माध्यम (ध्वनि, व्यंजना)
-
काव्य का औचित्य और कलात्मकता
-
सहृदय पाठक की तन्मयता
इन सभी के समुचित संयोग से ही रस निष्पन्न होता है।
उदाहरण: श्रृंगार रस की निष्पत्ति
यदि किसी कविता में नायक और नायिका की प्रणयवेला का चित्रण हो (आलंबन विभाव), चंद्रमा की शीतलता, फूलों की सुगंध, कोयल की कूक आदि (उद्दीपन विभाव) हों, तो वे पाठक के भीतर अनुराग उत्पन्न करने में सहायक होंगे। यदि भाव की प्रकटीकरण क्रियाएँ (अनुभाव)—जैसे, दृष्टि की लज्जा, हँसी, इशारे—भी समुचित हों, तो पाठक के भीतर श्रृंगार रस निष्पन्न हो सकता है—यदि वह सहृदय है।
निष्कर्ष
रस निष्पत्ति केवल एक सौंदर्यशास्त्रीय अवधारणा नहीं, बल्कि यह काव्य और पाठक के बीच एक गहन, अंतरंग संवाद की प्रक्रिया है। भरत ने इसके बीज बोए, परंतु इसका सैद्धांतिक विस्तार आनंदवर्धन, मम्मट और अभिनवगुप्त ने किया।
रस निष्पत्ति की प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि साहित्य केवल अर्थ या संदेश नहीं होता, वह अनुभव होता है—और यह अनुभव तभी संभव है जब पाठक उस साहित्य में अपने को भूलकर डूब जाए। अंत में यही कहा जा सकता है : “रस वह नहीं जो लिखा गया है, रस वह है जो भीतर जगा है।”
♦️वस्तुनिष्ठ प्रश्न♦️
1➤ ‘रस’ शब्द का मूल अर्थ क्या है?
2➤ भरत के अनुसार रस की उत्पत्ति किनसे होती है?
3➤ आलंबन विभाव क्या दर्शाता है?
4➤ उद्दीपन विभाव का उदाहरण कौन-सा है?
5➤ अनुभाव किसका प्रकटीकरण करते हैं?
6➤ ‘वाक्यार्थानुभवात् रसस्वादनम्’ किसका कथन है?
7➤ मम्मट के अनुसार रस की निष्पत्ति कहाँ होती है?
8➤ मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन-सा है?
9➤ ‘भावकता’ की संकल्पना किस आचार्य ने दी?
10➤ सहृदय पाठक की सबसे बड़ी योग्यता क्या होती है?
11➤ रस निष्पत्ति में ‘रचनात्मक सहभागिता’ किससे जुड़ी है?
12➤ ‘ध्वन्यालोक’ किस आचार्य की रचना है?
13➤ रस निष्पत्ति का उद्देश्य क्या है?