परिचय
मनोविश्लेषणवाद (Psychoanalysis) 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसकी स्थापना ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक सिग्मंड फ्रायड (Sigmund Freud) ने की थी। यह सिद्धांत व्यक्ति के अवचेतन मन, स्वप्न, यौन प्रवृत्तियों, अनुभवों और दमित इच्छाओं के विश्लेषण पर आधारित है। साहित्य में मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण पाठ्य-चरित्रों, घटनाओं और रचनाकार की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं की गहरी पड़ताल करता है। यह साहित्यिक रचना को मानव मन के दर्पण के रूप में देखता है।
मनोविश्लेषणवाद का उद्भव और विकास
1. सिग्मंड फ्रायड का योगदान

फ्रायड (1856–1939) ने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य का व्यवहार केवल चेतन मन (Conscious mind) से संचालित नहीं होता, बल्कि अवचेतन (Unconscious) और अचेतन (Subconscious) मन भी उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। फ्रायड के अनुसार मन तीन भागों में विभाजित है:
-
इड (Id): यह मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों (विशेषकर यौन और आक्रामक) का प्रतिनिधित्व करता है। यह बिना नैतिकता या तर्क के केवल इच्छा की पूर्ति चाहता है।
-
ईगो (Ego): यह वास्तविकता के आधार पर कार्य करता है और इड तथा सुपर-ईगो के बीच संतुलन बनाता है।
-
सुपर-ईगो (Super-ego): यह नैतिकता, सामाजिक मूल्य और आत्म-नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है।
2. अन्य मनोविश्लेषक विचारक
-
कार्ल गुस्ताव युंग (Carl Jung): युंग ने फ्रायड के विचारों से अलग होकर ‘सामूहिक अचेतन’ (Collective Unconscious) और ‘आर्केटाइप’ (Archetype) की अवधारणाएं दीं।
-
अल्फ्रेड एडलर (Alfred Adler): उन्होंने आत्म-संवर्धन और हीनता ग्रंथि (Inferiority Complex) की अवधारणाएं प्रस्तुत की।
-
एरिक फ्रॉम, जाक लोंका, और अना फ्रायड जैसे विचारकों ने मनोविश्लेषण की दिशा को विस्तृत किया।
मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख सिद्धांत
1. अवचेतन मन की भूमिका
अवचेतन मन में वे इच्छाएं, स्मृतियां और अनुभव छिपे होते हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
2. यौन प्रवृत्ति (Libido)
फ्रायड के अनुसार मनुष्य की प्रमुख प्रेरणा यौन ऊर्जा है। बाल्यावस्था में ही यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में कार्य करती है और यदि इसे दबाया जाए तो आगे चलकर मानसिक विकृति उत्पन्न होती है।
3. स्वप्न विश्लेषण
फ्रायड ने स्वप्नों को ‘अवचेतन की राह’ (The royal road to the unconscious) कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक The Interpretation of Dreams में बताया कि स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम हैं।
4. प्रतिरोध और दमन
मन जब किसी अस्वीकार्य विचार या इच्छा को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वह उसे दमन कर अवचेतन में भेज देता है। उपचार की प्रक्रिया में यह प्रतिरोध बनकर उभरता है।
साहित्य में मनोविश्लेषणवादी आलोचना
मनोविश्लेषणवादी आलोचना साहित्य को एक मानसिक उत्पाद मानती है। इसमें तीन मुख्य पक्षों का अध्ययन किया जाता है:
1. लेखक का मनोविश्लेषण
लेखक की जीवनी, बचपन के अनुभव, दबी हुई इच्छाएं और उसकी मानसिक अवस्था उसकी रचनाओं में प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए, दॉस्तोवस्की के उपन्यासों में अपराधबोध, मृत्यु की आशंका और दमन की प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं।
2. पात्रों का मनोविश्लेषण
कहानी या उपन्यास के पात्रों के व्यवहार, स्वप्न, भय, कुंठा, दमन और मानसिक संघर्षों की गहराई से जांच की जाती है।
उदाहरण: शेक्सपियर के हैमलेट का चरित्र – ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, आत्मसंघर्ष, और पिता की हत्या की इच्छा के रूप में विश्लेषित किया गया है।
3. पाठक का मनोविश्लेषण
पाठक किस प्रकार रचना से प्रभावित होता है, वह किन मानसिक अवस्थाओं से गुजरता है – यह भी मनोविश्लेषण का विषय है।
हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण
1. प्रेमचंद की कहानियाँ
प्रेमचंद की रचनाएँ सामाजिक यथार्थ के साथ-साथ पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराइयों को भी उजागर करती हैं। उनकी कहानी ‘ईदगाह’ में हामिद का व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति, सामाजिक अनुभव और अवचेतन इच्छाओं का परिणाम है।
2. जैनेन्द्र कुमार
जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ और उपन्यास पात्रों के अंतर्मन को केंद्र में रखते हैं। उनका उपन्यास ‘सुनीता’ नारी मन की दुविधा, इच्छा और आत्मसंघर्ष को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करता है।
3. अज्ञेय
अज्ञेय की रचनाओं में आत्म-विश्लेषण, दार्शनिक प्रश्न और व्यक्ति के भीतर की उथल-पुथल प्रमुख है। ‘शेखर: एक जीवनी’ एक प्रकार का आत्ममनोविश्लेषण है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर झांकता है।
4. मोहन राकेश और नवीन युगीन नाटक
मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव हिंदी नाटकों में भी पड़ा। मोहन राकेश का ‘आषाढ़ का एक दिन’ पात्रों की दबी इच्छाओं, द्वंद्व और संकोच को उभारता है।
मनोविश्लेषण और मिथक
युंग द्वारा प्रतिपादित ‘आर्केटाइप’ अवधारणा साहित्य में मिथकों की भूमिका को रेखांकित करती है। युंग के अनुसार, मानवता का एक सामूहिक अचेतन होता है, जिसमें कुछ सार्वभौमिक प्रतीक (जैसे मां, नायक, छाया, पुनर्जन्म आदि) बसे होते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग साहित्य में अक्सर अज्ञात स्तर पर होता है।
मनोविश्लेषणवाद की आलोचना
-
अति-यौन केंद्रितता:
फ्रायड के सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर की गई कि उन्होंने सभी मानसिक प्रक्रियाओं की जड़ यौन प्रवृत्तियों को माना, जो अतिशयोक्ति है। -
वैज्ञानिक आधार का अभाव:
मनोविश्लेषण का बहुत-सा भाग अनुभवजन्य और काल्पनिक है। इसका पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया जा सका है। -
पश्चिमी संस्कृति पर आधारित:
फ्रायड के सिद्धांत यूरोपीय समाज और संस्कृति पर आधारित हैं, जिनका सीधे रूप में अन्य संस्कृतियों पर लागू होना कठिन है।
मनोविश्लेषणवाद का समकालीन प्रभाव
आज मनोविश्लेषण का प्रयोग साहित्य के साथ-साथ सिनेमा, कला, दर्शन और जनसंचार माध्यमों में भी हो रहा है। मनोचिकित्सा, परामर्श, फिल्म समीक्षा, और यहां तक कि राजनैतिक विश्लेषण में भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों जैसे मिर्च मसाला, सदमा, ब्लैक, हाईवे, तमाशा आदि में पात्रों की मानसिक जटिलताओं को मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से समझा जा सकता है।
निष्कर्ष
मनोविश्लेषणवाद एक ऐसी दृष्टि है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को प्रकाश में लाने का प्रयास करती है। यह न केवल साहित्य के अध्ययन को गहराई प्रदान करता है, बल्कि मानव मन की जटिलता को समझने में भी सहायक है। साहित्य में इसका प्रयोग रचना और पाठक के बीच एक गहरे संवाद की स्थापना करता है। हिंदी साहित्य में भी मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण ने रचनाओं को नए ढंग से पढ़ने और समझने का अवसर प्रदान किया है। यद्यपि इसकी सीमाएं हैं, फिर भी यह एक प्रभावशाली और बहुआयामी आलोचनात्मक पद्धति बनी हुई है।
♦️वस्तुनिष्ठ प्रश्न♦️
1➤ मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने की थी?
2➤ मनोविश्लेषण में ‘इड’ किसका प्रतिनिधित्व करता है?
3➤ फ्रायड के अनुसार मन के कितने भाग होते हैं?
4➤ ‘सुपर ईगो’ किसका प्रतिनिधित्व करता है?
5➤ ‘ईगो’ का मुख्य कार्य क्या होता है?
6➤ फ्रायड की किस पुस्तक में स्वप्नों का विश्लेषण किया गया है?
7➤ ‘सामूहिक अचेतन’ की संकल्पना किसने दी?
8➤ ‘हीनता ग्रंथि’ का विचार किसने प्रस्तुत किया?
9➤ ‘आर्केटाइप’ अवधारणा का संबंध किस विचारक से है?
10➤ ‘अना फ्रायड’ ने योगदान दिया —
11➤ फ्रायड की आलोचना किस कारण की जाती है?
12➤ मनोविश्लेषणवादी आलोचना किसे प्राथमिक मानती है?

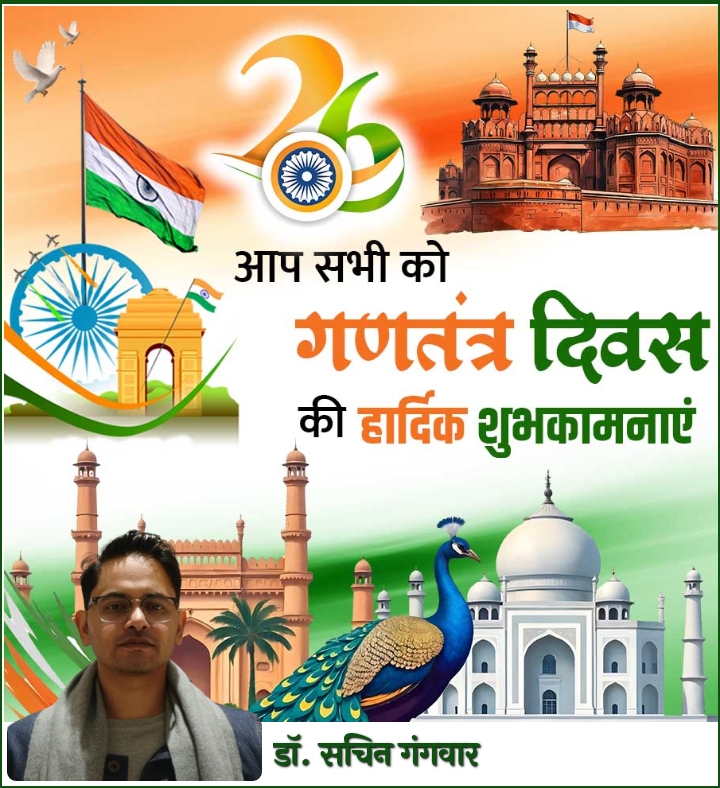

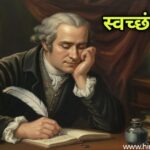



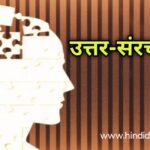
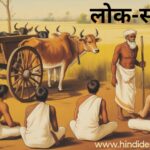




Ok