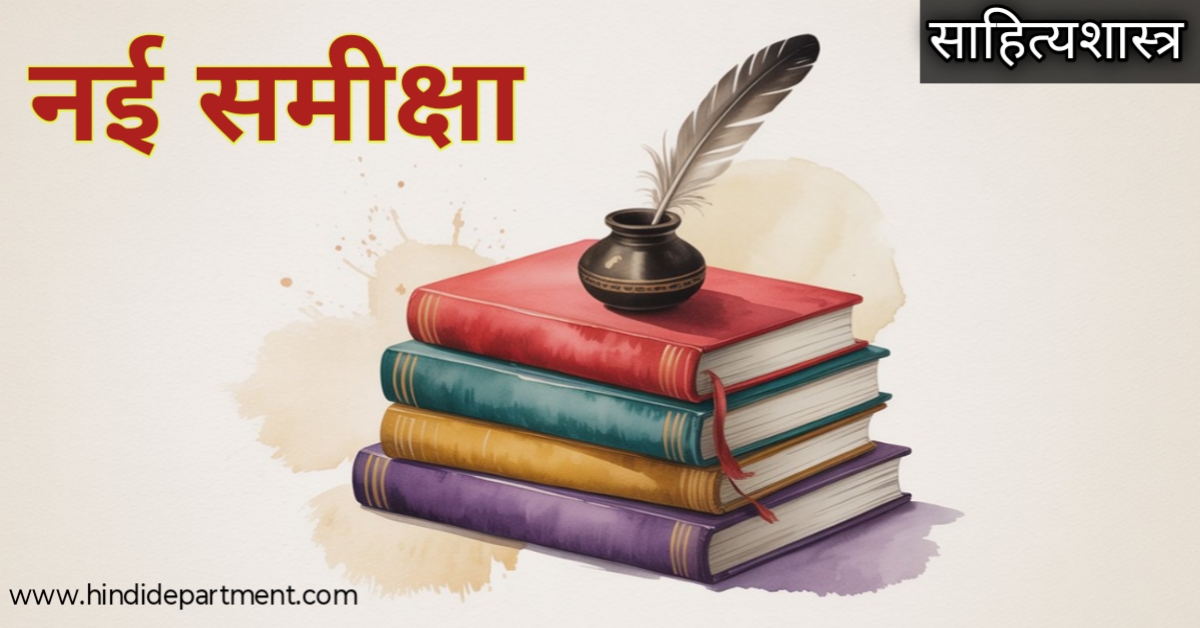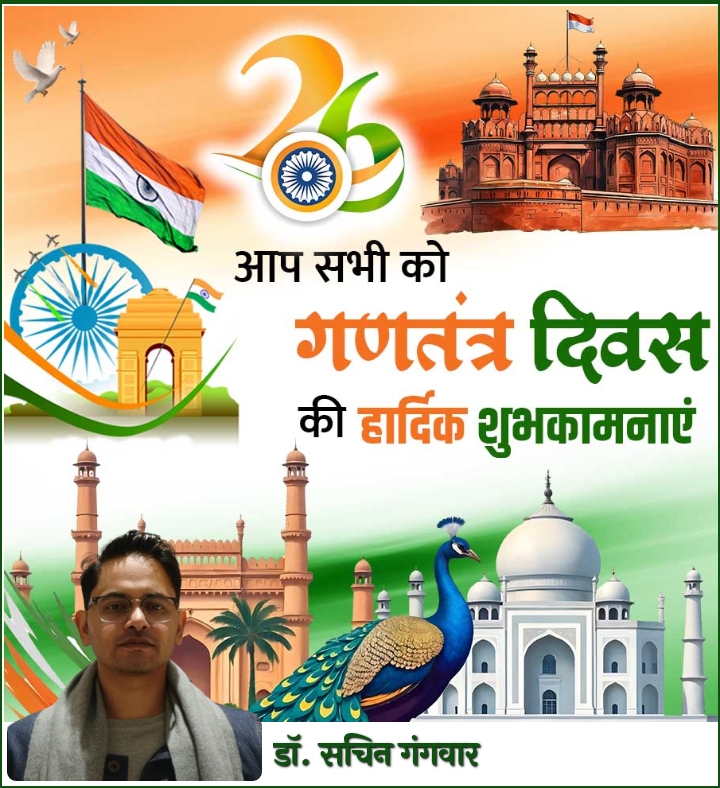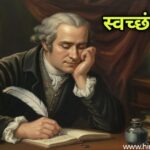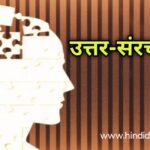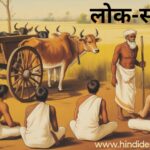प्रस्तावना
हिंदी साहित्य की आलोचना परंपरा में समय-समय पर अनेक दृष्टिकोण और प्रवृत्तियाँ उभरी हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस आलोचना पद्धति ने गंभीर ध्यान आकर्षित किया, वह है नई समीक्षा (New Criticism)। इसका उद्भव मुख्यतः अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में हुआ, परंतु इसके प्रभाव से हिंदी साहित्यिक विमर्श भी अछूता नहीं रहा। नई समीक्षा का मूल उद्देश्य साहित्यिक कृति को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखना और उसमें निहित अंतर्वस्तु, संरचना, प्रतीक योजना, भाषा प्रयोग तथा अर्थ के स्तरों की वस्तुनिष्ठ विवेचना करना रहा है।
यह आलोचना पद्धति पाठ-केंद्रित (Text-Centered) विश्लेषण की पक्षधर है और लेखक की जीवनी, ऐतिहासिक-सामाजिक परिस्थितियों या पाठक की प्रतिक्रियाओं को गौण मानती है। इस लेख में हम नई समीक्षा की अवधारणा, उसके प्रमुख सिद्धांत, प्रतिनिधि आलोचकों, हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव और इसकी सीमाओं का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।
नई समीक्षा की अवधारणा
नई समीक्षा (New Criticism) 1920 और 1930 के दशक में अमेरिका और इंग्लैंड में विकसित एक साहित्यिक आलोचना आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य काव्य की आंतरिक बनावट को परखना था, न कि बाहरी संदर्भों को। इस पद्धति के अनुसार कोई भी साहित्यिक रचना स्वयं में एक स्वतंत्र और पूर्ण संरचना होती है, जिसकी व्याख्या केवल उसके पाठ के आधार पर ही की जानी चाहिए।
नई समीक्षा “formalist” प्रवृत्ति से जुड़ी है, जिसमें विशेष बल संरचना, भाषिक उपकरणों, प्रतीकों, विरोधाभासों, संदर्भ और अर्थ की बहुस्तरीयता आदि पर दिया गया। यह रचना के “वाचिक” (verbal) तत्वों के सूक्ष्म विश्लेषण की अपेक्षा करती है।
नई समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत
-
पाठ की आत्मनिर्भरता (Autonomy of the Text):
नई समीक्षा मानती है कि साहित्यिक रचना को लेखक की मंशा, पाठक की प्रतिक्रिया या ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर नहीं, बल्कि स्वयं पाठ के भीतर से ही समझा जाना चाहिए। -
सघनता (Tension) और विरोधाभास (Paradox):
काव्य में अर्थ की विविधता और परतों को उजागर करने के लिए इन उपकरणों का विश्लेषण अनिवार्य है। विरोधाभासों के माध्यम से काव्य अपने जटिल और गहन अर्थ प्रस्तुत करता है। -
Irony और Ambiguity:
नई समीक्षा में काव्य की वक्रता और अस्पष्टता को काव्यात्मकता का मूल गुण माना गया। अर्थ की अस्पष्टता को इसमें कमजोरी नहीं, बल्कि साहित्यिक गुण माना। -
Close Reading:
पाठ का सूक्ष्म और बारीकी से अध्ययन, जिसमें प्रत्येक पंक्ति, शब्द और प्रतीक का विश्लेषण किया जाता है। -
Intentional Fallacy और Affective Fallacy:
ये दो भ्रांतियाँ नई समीक्षा के अनुसार आलोचना में बाधा बनती हैं—-
Intentional Fallacy: लेखक की मंशा का अनुमान लगाना अनुचित है।
-
Affective Fallacy: पाठक की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के आधार पर काव्य को समझना ग़लत है।
-
नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक
-
आई.ए. रिचर्ड्स (I. A. Richards):
उन्होंने ‘Practical Criticism’ और ‘Principles of Literary Criticism’ जैसी पुस्तकों में साहित्यिक भाषा, अर्थ, और संप्रेषण पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। -
टी. एस. इलियट (T. S. Eliot):
उन्होंने परंपरा और व्यक्तित्व की अवधारणा दी। कविता की निरपेक्षता और वस्तुनिष्ठ सहमिति (Objective Correlative) जैसे विचारों से नई समीक्षा को आधार प्रदान किया। -
क्लीन्थ ब्रूक्स (Cleanth Brooks):
उन्होंने ‘The Well-Wrought Urn’ जैसी कृति में काव्य की संरचना और उसके विरोधाभासों पर बल दिया। -
विलियम एम्पसन (William Empson):
उन्होंने ‘Seven Types of Ambiguity’ में काव्य की भाषिक जटिलता और बहुस्तरीयता का विश्लेषण प्रस्तुत किया। -
जॉन क्रो रैनसम (John Crowe Ransom):
उन्होंने ‘नई समीक्षा’ शब्द को प्रचारित किया और इस विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता बने।
हिंदी आलोचना पर नई समीक्षा का प्रभाव
हिंदी आलोचना में नई समीक्षा का प्रभाव 1950 के दशक के बाद देखने को मिलता है। भारत में अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षित आलोचक और कवि इस पद्धति से प्रभावित हुए। हिंदी आलोचना में नंददुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह (शुरुआती काल), डॉ. नगेन्द्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि आलोचकों ने कहीं न कहीं नई समीक्षा के उपकरणों का प्रयोग अवश्य किया।
1. नगेन्द्र और नई समीक्षा:
डॉ. नगेन्द्र ने हिंदी आलोचना में नई समीक्षा के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया। उनकी पुस्तकों और लेखों में काव्य की आंतरिक बनावट, रूपात्मक सौंदर्य, प्रतीकों आदि का विश्लेषण मिलता है।
2. आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विपरीत:
शुक्ल जी की ऐतिहासिक-सामाजिक पद्धति नई समीक्षा से विपरीत थी। शुक्ल जी ने साहित्य को युगचेतना और समाज के साथ जोड़कर देखा, जबकि नई समीक्षा काव्य को आत्मनिर्भर मानती है।
3. समकालीन आलोचना में प्रयोग:
आज भी कविता के विश्लेषण में ‘क्लोज़ रीडिंग’, ‘प्रतीक योजना’, ‘विरोधाभास’ आदि तत्वों का उपयोग अनेक अध्येता और आलोचक करते हैं, जो नई समीक्षा की देन है।
नई समीक्षा की उपादेयता
-
साहित्यिक शुद्धता की ओर उन्मुखता:
इसने आलोचना को बाह्य विचारों से हटाकर साहित्यिक शिल्प और सौंदर्य की ओर मोड़ा। -
साहित्य को आत्मनिर्भर दृष्टि से देखने का आग्रह:
पाठ के भीतर के संकेतों और संरचनात्मक गूढ़ताओं को समझने में सहायक। -
काव्य के गूढ़ अर्थों की खोज:
प्रतीक, विरोधाभास, विडंबना जैसे उपकरणों के विश्लेषण से पाठ की बहुस्तरीय व्याख्या संभव हुई। -
प्रशिक्षणात्मक दृष्टि:
आलोचकों को सटीक और गहराईपूर्ण अध्ययन करने की दिशा में प्रेरित किया।
नई समीक्षा की सीमाएँ
-
सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों की उपेक्षा:
यह आलोचना रचना को समाज, इतिहास और राजनीति से काट देती है। -
लेखक और पाठक की भूमिका की उपेक्षा:
लेखक की मंशा और पाठक की प्रतिक्रिया साहित्य में महत्त्वपूर्ण होती है, जिसे नई समीक्षा नकार देती है। -
सिर्फ काव्य पर केंद्रित दृष्टिकोण:
यह गद्य, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं के विश्लेषण में उतनी प्रभावी नहीं रही। -
वर्गीय, लैंगिक, जातीय विमर्शों की अनदेखी:
दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, उत्तरवर्ती आलोचना प्रवृत्तियों में इसकी उपयोगिता सीमित है।
उत्तर आधुनिक युग में नई समीक्षा की प्रासंगिकता
आज के उत्तर आधुनिक समय में जहाँ विमर्शधर्मी आलोचना प्रचलन में है, वहाँ नई समीक्षा का स्थान थोड़ा सीमित हो गया है। परंतु फिर भी पाठ की सूक्ष्म व्याख्या, प्रतीकों की पहचान, और भाषिक संरचना का गहन विश्लेषण करने के लिए इसकी पद्धति आज भी उपयोगी मानी जाती है। आधुनिक शिक्षण संस्थानों में ‘क्लोज़ रीडिंग’ एक आवश्यक कौशल बना हुआ है।
निष्कर्ष
नई समीक्षा ने साहित्यिक आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। इसने पाठ को केंद्र में रखकर साहित्यिक विश्लेषण की एक स्वायत्त और वैज्ञानिक पद्धति विकसित की, जिसने साहित्य को केवल ऐतिहासिक या सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र कलात्मक संरचना के रूप में देखने की दृष्टि दी। यद्यपि इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट हैं, फिर भी यह पद्धति आज भी साहित्यिक अध्ययन और शिक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी आलोचना ने भी इससे बहुत कुछ ग्रहण किया है और यह आज भी कविता-विश्लेषण की एक मजबूत आधारभूमि है।
♦️वस्तुनिष्ठ प्रश्न♦️
1➤ नई समीक्षा का उद्भव किस दशक में हुआ था?
2➤ नई समीक्षा किस प्रकार की आलोचना पद्धति है?
3➤ नई समीक्षा किस तत्त्व को मुख्य रूप से महत्त्व देती है?
4➤ “Close Reading” शब्द किस आलोचना पद्धति से संबंधित है?
5➤ ‘Affective Fallacy’ का क्या अर्थ है?
6➤ “The Well-Wrought Urn” के लेखक कौन हैं?
7➤ “Seven Types of Ambiguity” पुस्तक किसने लिखी?
8➤ Objective Correlative की अवधारणा किसने दी?
9➤ नई समीक्षा किस प्रकार की आलोचना को अस्वीकार करती है?
10➤ नई समीक्षा किस प्रकार की दृष्टि को बढ़ावा देती है?
11➤ ‘नई समीक्षा’ के अनुसार कविता क्या है?
12➤ नई समीक्षा के आलोचकों का मुख्य कार्य क्या था?
13➤ नई समीक्षा आज किस रूप में उपयोगी मानी जाती है?