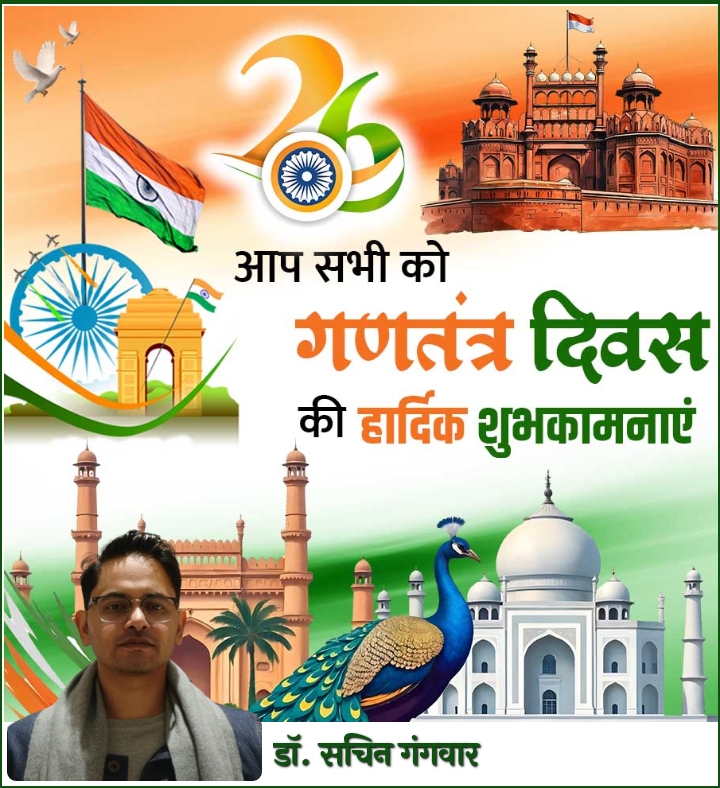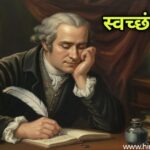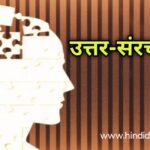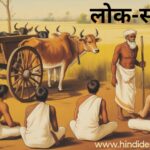जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ‘चंद्रगुप्त‘ हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है, जिसका प्रकाशन 1931 ई. में हुआ था। यह नाटक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, उनके उत्थान और भारत में विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष की कथा को प्रस्तुत करता है।
नाटक का परिचय
-
रचनाकार: जयशंकर प्रसाद
-
प्रकाशन वर्ष: 1931 ई.
-
अंक: 4
-
दृश्य: 44
-
गीतों की संख्या: 13
-
पात्रों की संख्या: 35 (24 पुरुष, 11 स्त्री)
-
मुख्य विषय: मौर्य साम्राज्य की स्थापना, विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार, राष्ट्रवाद, कूटनीति, प्रेम और बलिदान।
लेखक का परिचय

प्रमुख पात्र
पुरुष पात्र
-
चंद्रगुप्त मौर्य: नाटक के नायक; साहसी, आत्मविश्वासी और राष्ट्रभक्त।
-
चाणक्य (विष्णुगुप्त): राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीति के प्रतीक; मौर्य साम्राज्य के निर्माता।
-
नंद: मगध का विलासी और अत्याचारी राजा।
-
राक्षस: मगध का अमात्य; सुवासिनी का प्रेमी।
-
वररुचि (कात्यायन): मगध का विद्वान अमात्य।
-
शकटार: मगध का मंत्री।
-
आंभीक: तक्षशिला का राजकुमार; सिकंदर का सहयोगी।
-
सिंहरण: मालव गण का प्रमुख; अलका का प्रेमी।
-
पर्वतेश्वर: पंजाब का राजा; सिकंदर से युद्ध करता है।
-
सिकंदर: यूनानी विजेता; भारत पर आक्रमण करता है।
-
फिलिप्स: सिकंदर का क्षत्रप।
-
सिल्यूकस: सिकंदर का सेनापति; बाद में चंद्रगुप्त से पराजित होता है।
स्त्री पात्र
-
अलका: गांधार की राजकुमारी; राष्ट्रप्रेमी और साहसी।
-
सुवासिनी: शकटार की कन्या; राक्षस की प्रेमिका।
-
कल्याणी: मगध की राजकुमारी।
-
मालविका: सिंधु देश की राजकुमारी; चंद्रगुप्त की प्रेमिका।
-
कार्नेलिया: सिल्यूकस की पुत्री; चंद्रगुप्त से विवाह करती है।
-
नीला और लीला: कल्याणी की सहेलियाँ।
चंद्रगुप्त (नाटक)
कथासार
प्रथम अंक
-
तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण और आंभीक की वार्तालाप से नाटक का आरंभ होता है।
-
चाणक्य मगध के राजा नंद से अपमानित होकर प्रतिशोध की शपथ लेता है।
-
चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की योजना बनाते हैं।
द्वितीय अंक
-
पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण और पर्वतेश्वर का प्रतिकार।
-
चंद्रगुप्त मालव और तक्षशिला की सेनाओं का नेतृत्व करता है।
-
सिकंदर घायल होता है; चंद्रगुप्त उसे प्राणदान देता है।
तृतीय अंक
-
चाणक्य की कूटनीति से राक्षस और अन्य मगध के मंत्री चंद्रगुप्त के पक्ष में आते हैं।
-
नंद की हत्या के बाद चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता है।
चतुर्थ अंक
-
पर्वतेश्वर और कल्याणी की मृत्यु; मालविका का बलिदान।
-
सिल्यूकस का आक्रमण और पराजय; कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से विवाह।
-
चाणक्य राजनीति से संन्यास लेता है।
गीत योजना
-
नाटक में कुल 13 गीत हैं: प्रथम अंक में 2, द्वितीय में 3, तृतीय में 1, और चतुर्थ में 7।
-
प्रसिद्ध गीत: “अरुण यह मधुमय देश हमारा” (कार्नेलिया द्वारा गाया गया), “हिमाद्रि तुंग श्रृंग से” (अलका द्वारा गाया गया)।
-
गीतों के माध्यम से पात्रों की भावनाओं और राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति होती है।
प्रमुख उद्धरण
1. चाणक्य
“मौर्य! तुम्हारा पुत्र आज आर्यावर्त्त का सम्राट है—अब और कौन-सा सुख तुम देखना चाहते हो? काषाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा।”
विश्लेषण: यह उद्धरण चाणक्य की प्रतिज्ञा और कर्म-संयम की शिक्षा देता है— इसमें सत्ता मिलने के बाद भी आत्मा की विनम्रता बनाए रखने की सीख मिलती है।
2. चंद्रगुप्त
“मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शान्ति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए, मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए।”
विश्लेषण: चंद्रगुप्त की दृष्टि स्पष्ट करती है कि किसी भी कृत्य में साधन का महत्व परिणामों से भी अधिक होता है। वह राष्ट्र-भक्ति में तात्कालिक कठोरता को आवश्यक मानता है।
3. चाणक्य
“चाणक्य : चन्द्रगुप्त! मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। … सन्तोष धन था।”
विश्लेषण: चाणक्य स्वयं की आत्म-परिभाषा इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसके लिए राज्य सत्ता करुणा से संचालित होती है, धर्म प्रेम से और सन्तोष ही सच्चा धन है।
4. चंद्रगुप्त
“स्वतन्त्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं।”
विश्लेषण: यह उद्धरण राष्ट्र-प्रेम की एकता को रेखांकित करता है—युद्ध में पद, प्रतिष्ठा या पदानुक्रम मायने नहीं रखते, बल्कि उद्देश्य ही मूर्तिमान होता है।
5. चाणक्य
“चाणक्य सिद्धि देखता है साधन चाहे कैसे ही हों।”
विश्लेषण: उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन उचित हो सकता है, यह उनकी कूटनीतिक मानसिकता है।
6. कार्नेलिया
“कार्नेलिया : सिकन्दर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। … यह अरस्तू और चाणक्य चोट है, सिकन्दर और चन्द्रगुप्त उनके अस्त्र हैं।”
विश्लेषण: इस उद्धरण में भारतीयता और विदेशी ज्ञान की तुलना विस्तार से कही गई है। इसमें ज्ञान और शक्ति का सम्मिश्रण दर्शाया गया है।
♦️वस्तुनिष्ठ प्रश्न♦️
1➤ ‘चंद्रगुप्त’ नाटक के रचयिता कौन हैं?
2➤ ‘चंद्रगुप्त’ नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था?
3➤ इस नाटक में कुल कितने अंक हैं?
4➤ अलका किस राज्य की राजकुमारी है?
5➤ नंद कौन था?
6➤ ‘अरुण यह मधुमय देश हमारा’ गीत किस पात्र ने गाया है?
7➤ नाटक का मुख्य विषय क्या है?
8➤ ‘हिमाद्रि तुंग श्रृंग से’ गीत किस पात्र द्वारा गाया गया है?
9➤ सिकंदर का सेनापति कौन है?
10➤ जयशंकर प्रसाद का संबंध किस युग से है?
11➤ ‘स्वतन्त्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं’ – यह किसका कथन है?
12➤ ‘मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए…’ यह कथन किसका है?
13➤ कार्नेलिया किसकी पुत्री है?
14➤ आंभीक किसका सहयोगी था?
15➤ ‘चंद्रगुप्त’ नाटक में राष्ट्रवाद की भावना किस रूप में प्रकट होती है?