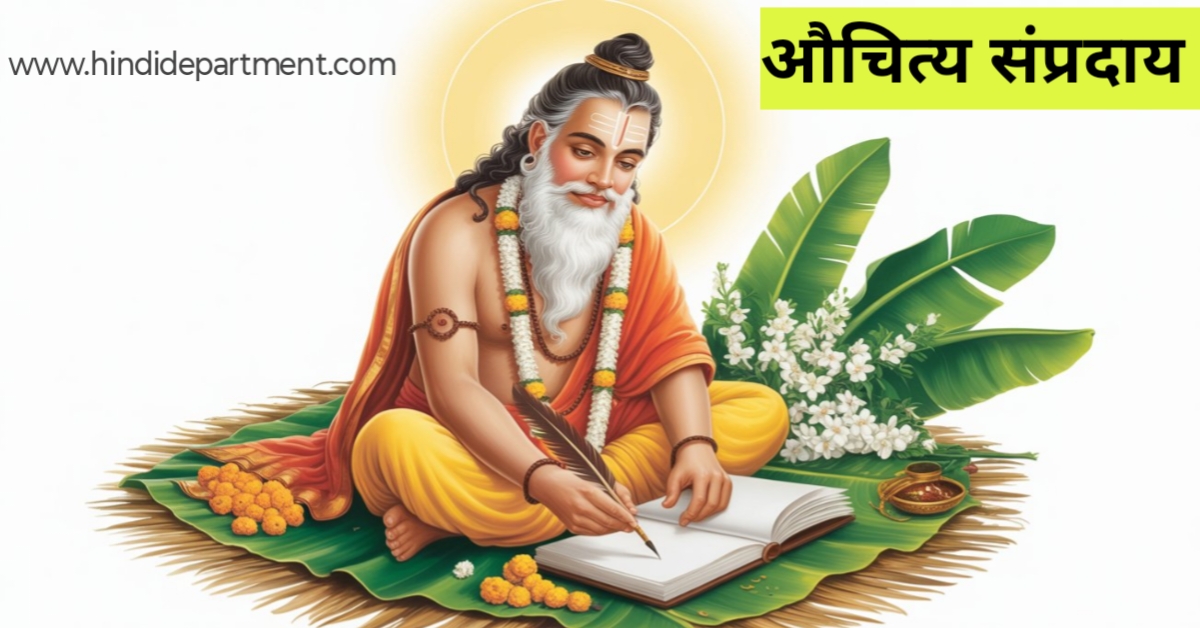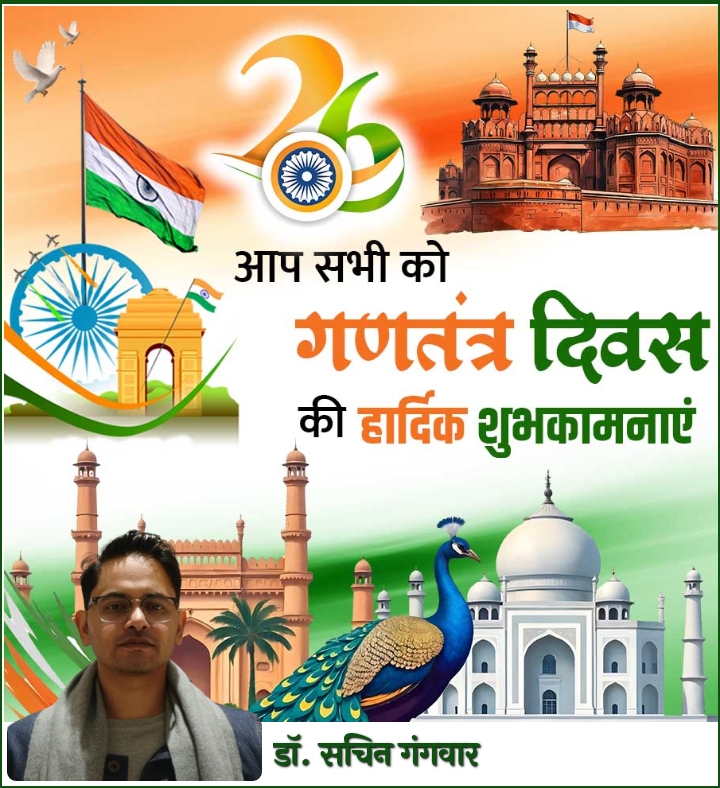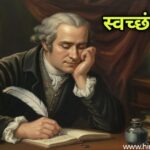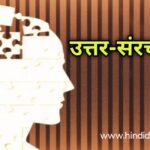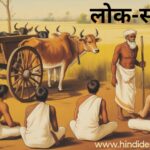प्रस्तावना
भारतीय दर्शन की विविध धाराओं में औचित्य संप्रदाय (auchitya sampradaya) एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और काव्य-मीमांसीय अवधारणा है, जिसे महाकवि क्षेमेन्द्र द्वारा व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह संप्रदाय काव्यशास्त्र की वह धारा है जो काव्य में औचित्य (उचितता) की प्रमुखता पर बल देती है। क्षेमेन्द्र की प्रसिद्ध कृति औचित्य विचार चर्चा इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी काव्य रचना में भाव, शब्द, पात्र, देश, काल और प्रसंग—इन सभी के संदर्भ में उपयुक्तता अत्यंत आवश्यक है। इस लेख में हम औचित्य संप्रदाय की उत्पत्ति, मूल तत्व, साहित्यिक महत्त्व, इसकी आधुनिक प्रासंगिकता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे।
1. औचित्य का अर्थ और परिभाषा
औचित्य का सामान्य अर्थ है “उचित होना” या “योग्यता के अनुरूप होना।” काव्यशास्त्र में यह शब्द उस सौंदर्यशास्त्रीय नियम की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार किसी भी साहित्यिक या कलात्मक रचना के विभिन्न अंगों का आपसी समन्वय आवश्यक है।
क्षेमेन्द्र के अनुसार:
“औचित्यं नाम सर्वत्र कार्यं काव्येषु निर्मले।
यथा पात्रक्रियावर्णप्रसङ्गवचनादिषु॥”
— अर्थात् काव्य के शुद्ध रूप में औचित्य का सर्वत्र होना आवश्यक है, चाहे वह पात्र, क्रिया, वर्णन, प्रसंग या वचन के संदर्भ में हो।
2. औचित्य संप्रदाय का उद्भव और विकास
औचित्य संप्रदाय की अवधारणा को सबसे पहले क्षेमेन्द्र (11वीं शताब्दी) ने सुस्पष्ट रूप में रखा। क्षेमेन्द्र ने अपनी कृति औचित्य विचार चर्चा में काव्य के विभिन्न तत्वों में औचित्य की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काव्य में कोई भी ऐसा तत्त्व नहीं होना चाहिए जो पात्र, स्थिति, काल, या सामाजिक नियमों के प्रतिकूल हो।
क्षेमेन्द्र का उद्देश्य केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि उन्होंने काव्य को एक नैतिक और सामाजिक अनुशासन की दृष्टि से भी देखा। उनके अनुसार काव्य का सौंदर्य तभी पूर्ण होता है जब वह युक्तियुक्त और सुसंगत हो।
3. औचित्य संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत
(क) पात्रानुरूपता :
किसी भी रचना में पात्र की उम्र, लिंग, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, संस्कार, और मनोभाव के अनुसार उसकी भाषा और कार्यों का निर्धारण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध ब्राह्मण पात्र के मुख से अशिष्ट शब्द उचित नहीं माने जाएंगे।
(ख) देश-काल औचित्य :
कविता या नाटक का घटनाक्रम जिस समय और स्थान से संबंधित है, उसी के अनुरूप भाषा, पहनावा, व्यवहार और रीति-नीति का चित्रण होना चाहिए। जैसे—राजस्थानी परिवेश में बंगाल की वेशभूषा असंगत होगी।
(ग) वृत्ति और भाषा औचित्य :
कविता में प्रयुक्त भाषा, शैली और वृत्त (verse) रचना के भावों और उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। वीर रस के प्रसंग में कोमल भावनाओं या शृंगार रस की शब्दावली अनुपयुक्त मानी जाएगी।
(घ) रस और भावों में औचित्य :
रसों की अभिव्यक्ति में भी औचित्य का पालन आवश्यक है। जहाँ करुण रस प्रमुख है वहाँ हास्य या वीभत्स का प्रयोग अनुचित माना जाता है।
(ङ) संयम और मर्यादा का औचित्य :
क्षेमेन्द्र ने काव्य में अनावश्यक अश्लीलता, अतिरंजना और अतिरेक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि काव्य को संस्कारयुक्त होना चाहिए।
4. औचित्य संप्रदाय की अन्य काव्य संप्रदायों से तुलना
(क) ध्वनि संप्रदाय (आनंदवर्धन) :
ध्वनि संप्रदाय में रस और व्यंजना को प्रधान माना गया है, जबकि औचित्य संप्रदाय में काव्य के सभी तत्त्वों की उचित संगति पर बल दिया गया है। ध्वनि संप्रदाय में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता महत्वपूर्ण है, जबकि औचित्य संप्रदाय में अभिव्यक्ति की उपयुक्तता।
(ख) रीति संप्रदाय (वामन) :
रीति संप्रदाय काव्य की शैली (रीति) को प्रधान तत्व मानता है। औचित्य संप्रदाय में शैली भी महत्वपूर्ण है, परन्तु केवल तभी जब वह पात्र और विषयवस्तु के अनुरूप हो।
(ग) अलंकार संप्रदाय (भामह आदि) :
जहाँ अलंकार संप्रदाय काव्य के सौंदर्य को विशेषणों और अलंकारों में खोजता है, वहीं औचित्य संप्रदाय अलंकारों के प्रयोग को भी युक्तिसंगत और आवश्यकतानुसार सीमित रखता है।
5. औचित्य संप्रदाय का साहित्यिक महत्त्व
(क) काव्य की वास्तविकता और स्वाभाविकता का आधार :
औचित्य संप्रदाय काव्य को वास्तविकता के धरातल पर बनाए रखता है। यह कल्पना की उड़ानों को भी सीमाओं में रखता है, जिससे काव्य अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनता है।
(ख) सामाजिक और नैतिक अनुशासन की स्थापना :
औचित्य संप्रदाय के माध्यम से क्षेमेन्द्र ने काव्य को सामाजिक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ा। इससे काव्य केवल मनोरंजन का साधन न होकर, शिक्षाप्रद और समाजोपयोगी बनता है।
(ग) काव्य-समीक्षा का मानदंड :
औचित्य संप्रदाय ने काव्य समीक्षा के लिए एक ठोस मानदंड दिया है। इससे किसी भी रचना की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सकता है।
6. औचित्य संप्रदाय की आधुनिक प्रासंगिकता
आज के साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में, जब अनुशासनहीनता को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना जा रहा है, तब भी औचित्य संप्रदाय की प्रासंगिकता बनी हुई है। विशेषतः निम्नलिखित कारणों से:
(क) फिल्मों, नाटकों और उपन्यासों में यथार्थ का प्रश्न :
किसी भी माध्यम में जब पात्रों का आचरण अस्वाभाविक हो या संवाद उनके चरित्र से मेल न खाएं, तब उनकी विश्वसनीयता घट जाती है। औचित्य संप्रदाय ऐसी विसंगतियों की पहचान करने में मदद करता है।
(ख) साहित्यिक आलोचना और शिक्षण :
औचित्य संप्रदाय साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन में आज भी उपयोगी है। यह छात्रों और समीक्षकों को एक ठोस कसौटी देता है।
(ग) सांस्कृतिक सरंक्षण :
भारतीय काव्य परंपरा में जो संयम, मर्यादा और धर्मबुद्धि है, औचित्य संप्रदाय उसके संरक्षण में सहायक है।
7. औचित्य संप्रदाय पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण
हालाँकि औचित्य संप्रदाय एक संतुलित काव्य दृष्टिकोण प्रदान करता है, परंतु कुछ आलोचक इसे रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश मानते हैं। उनके अनुसार, कल्पना की उड़ानों को औचित्य की कसौटी पर कसा जाना रचनाकार की स्वच्छंदता को बाधित करता है।
आधुनिकतावादी और प्रयोगवादी कवि इसे एक रूढ़ दृष्टिकोण मानते हैं, जो साहित्य को परंपरा में बाँधने का कार्य करता है। उनके अनुसार, औचित्य का मापदंड कालानुसार बदलता रहता है, अतः कोई एक सार्वभौमिक औचित्य संभव नहीं है।
8. निष्कर्ष
औचित्य संप्रदाय भारतीय काव्य परंपरा की एक ऐसी धारा है जिसने साहित्य को एक संतुलित, सुसंगत और नैतिक अनुशासन में ढालने का प्रयास किया। क्षेमेन्द्र की दृष्टि में साहित्य केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक दिशा देने का माध्यम है। यद्यपि आधुनिक समय में औचित्य की धारणा अधिक लचीली हो गई है, फिर भी औचित्य संप्रदाय की मूल भावना आज भी प्रासंगिक है—विशेषतः तब, जब साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और मानव मन की गहराइयों तक पहुँचना हो।
इस प्रकार, औचित्य संप्रदाय न केवल साहित्यिक विवेक का प्रतीक है, बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य-व्यवस्था को भी प्रतिष्ठित करता है। इसे समझना और अपनाना साहित्य को अधिक सार्थक, स्वाभाविक और प्रभावशाली बना सकता है।
♦️वस्तुनिष्ठ प्रश्न♦️
1➤ औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है?
2➤ ‘औचित्य विचार चर्चा’ ग्रंथ के रचयिता कौन हैं?
3➤ ‘औचित्य’ शब्द का सामान्य अर्थ है—
4➤ औचित्य संप्रदाय किस बात पर विशेष बल देता है?
5➤ “औचित्यं नाम सर्वत्र कार्यं काव्येषु निर्मले…” यह कथन किसका है?
6➤ औचित्य संप्रदाय में ‘पात्रानुरूपता’ का तात्पर्य है—
7➤ औचित्य संप्रदाय में काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए?
8➤ औचित्य संप्रदाय में किस प्रकार की कल्पना को अस्वीकार किया गया है?
9➤ औचित्य संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
10➤ किस दृष्टिकोण से औचित्य संप्रदाय आधुनिक समय में भी उपयोगी है?
11➤ आलोचकों के अनुसार औचित्य संप्रदाय की एक कमजोरी क्या है?
12➤ औचित्य संप्रदाय के अनुसार ‘नायक’ की भाषा कैसी होनी चाहिए?
13➤ औचित्य संप्रदाय किस शास्त्र से जुड़ा है?
14➤ औचित्य का स्वरूप कैसा माना जाता है?
15➤ आज के संदर्भ में औचित्य संप्रदाय किसमें सहायक है?