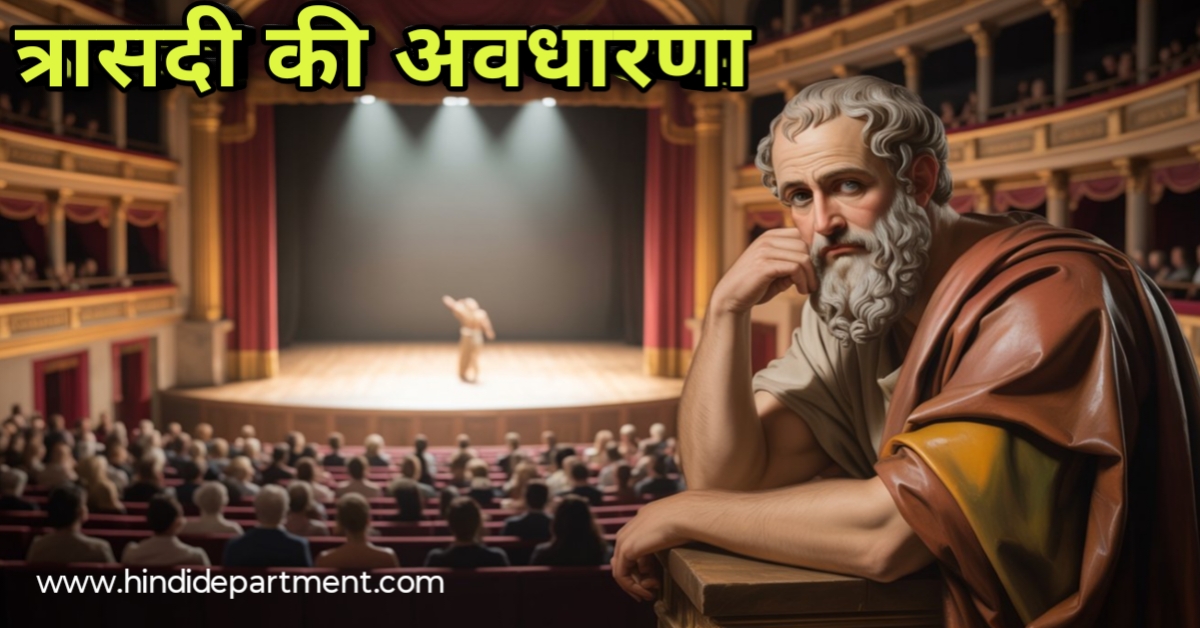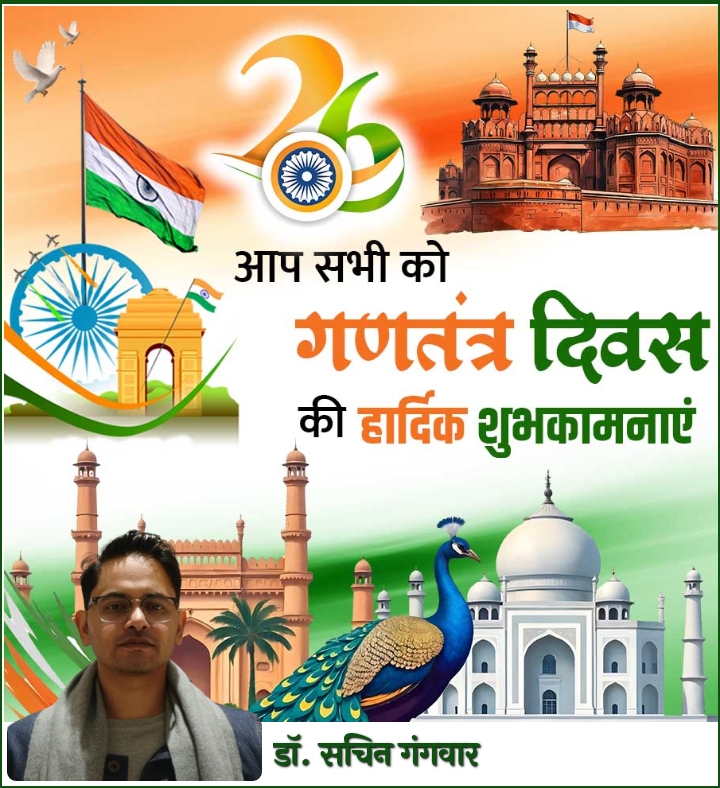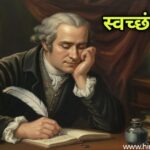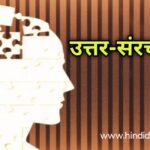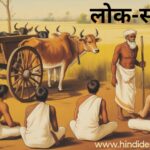प्रस्तावना
त्रासदी (Tragedy) मूल रूप से नाटकों की एक शैली है जिसमें हमें मानवीय दुःखों का वर्णन देखने को मिलता है। इस तरह के नाटकों का मुख्य उद्धेश्य दर्शकों के भावों को शुद्ध करना होता है। इसका गहन और वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु (Aristotle) ने अपने ग्रंथ ‘Poetics’ में किया। अरस्तु का त्रासदी संबंधी विवेचन न केवल प्राचीन यूनानी नाट्य परंपरा की व्याख्या करता है, बल्कि यह विश्व साहित्य की त्रासदी संबंधी अवधारणाओं की आधारशिला भी बन गया है। उनका यह विवेचन आज भी नाटक और नाट्यशास्त्र के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक माना जाता है।
इस लेख में अरस्तु के त्रासदी संबंधी विचारों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
1. अरस्तु की त्रासदी की परिभाषा
अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है:
“Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the catharsis of such emotions.”
हिंदी अनुवाद:
“त्रासदी गंभीर, पूर्ण और निश्चित आकार की किसी क्रिया का अनुकरण है, जिसे अलंकारयुक्त भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कथा के रूप में न होकर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, और जिसका उद्देश्य करुणा और भय के माध्यम से उन भावनाओं की शुद्धि (कैथार्सिस) करना होता है।”
इस परिभाषा से स्पष्ट है कि त्रासदी केवल दुखद घटनाओं की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि एक कलात्मक और उद्देश्यपूर्ण संरचना है, जो दर्शकों के भावों को उद्वेलित कर अंततः उन्हें शुद्ध करती है।
2. अनुकरण (Mimesis)
अरस्तु के अनुसार काव्य का मूल कार्य “अनुकरण” (Mimesis) है। त्रासदी भी जीवन की गंभीर और महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुकरण है। यह अनुकरण केवल वास्तविक घटनाओं की नकल नहीं है, बल्कि उसे एक कलात्मक और सृजनात्मक रूप देना है जिससे सत्य की अनुभूति हो सके।
त्रासदी में अनुकरण का उद्देश्य है – चरित्रों की गतिविधियों, उनके निर्णयों और उनके नैतिक संघर्षों का जीवन्त रूप से चित्रण करना। यह चित्रण दर्शकों को जीवन की जटिलताओं से परिचित कराता है।
3. त्रासदी के अनिवार्य अंग
अरस्तु ने त्रासदी के छः अंगों का उल्लेख किया है:
-
कथावस्तु (Plot / Mythos)
-
चरित्र (Character / Ethos)
-
विचार (Thought / Dianoia)
-
भाषा (Diction / Lexis)
-
गायन (Melody / Melos)
-
दृश्यविधान (Spectacle / Opsis)
इनमें से कथावस्तु को अरस्तु ने सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि वही संपूर्ण नाटक की आत्मा होती है।
3.1 कथावस्तु (Plot)
त्रासदी की कथावस्तु एक सुसंगठित, पूर्ण और संगठित क्रिया होनी चाहिए, जिसमें आरंभ, मध्य और अंत हो। इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि घटनाएँ आपस में आवश्यक और संभाव्य कारण-परिणाम संबंधों से जुड़ी हों।
अरस्तु ने त्रासदी के दो महत्वपूर्ण प्रकारों का उल्लेख किया है:
-
सरल त्रासदी (Simple Tragedy): जिसमें कोई विशेष उलटफेर (Peripeteia) या पहचान (Anagnorisis) नहीं होती।
-
जटिल त्रासदी (Complex Tragedy): जिसमें कथानक में उलटफेर और पहचान के तत्व होते हैं, जिससे दर्शकों में अधिक गहन भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।
3.2 चरित्र (Character)
चरित्रों का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वे विश्वसनीय, सुसंगत और नैतिक दृष्टि से गंभीर हों। त्रासदी का नायक न तो पूर्णतः पुण्यात्मा होता है और न ही पूर्णतः पापी। वह एक सामान्य व्यक्ति होता है, जिसमें कोई त्रुटि (Hamartia) होती है, जिसके कारण वह विनाश की ओर बढ़ता है।
यह त्रुटि मानवीय होती है, जिससे दर्शक नायक के प्रति करुणा और भय की भावना महसूस करते हैं।
3.3 विचार (Thought)
विचार से तात्पर्य है – संवादों के माध्यम से प्रस्तुत विचारधारा, नैतिकता, तर्क और भावनाएं। यह लेखक की दार्शनिक दृष्टि को दर्शाती है।
3.4 भाषा (Diction)
नाटक की भाषा प्रभावशाली, सुंदर, और पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। त्रासदी की भाषा में लय, प्रतीक, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारिक तत्वों का समावेश होना चाहिए।
3.5 गायन (Melody)
प्राचीन यूनानी नाटकों में गायन का विशेष स्थान था। कोरस के माध्यम से नाट्य भाव को गहराई मिलती थी। संगीत और गायन दर्शकों के भावों को जाग्रत करने का सशक्त माध्यम था।
3.6 दृश्यविधान (Spectacle)
दृश्यविधान से तात्पर्य मंच पर होने वाली दृश्यात्मक प्रस्तुतियों से है – जैसे प्रकाश, वेशभूषा, रंगमंच सज्जा आदि। अरस्तु ने इसे सबसे निम्न स्तर का तत्व माना है, क्योंकि यह नाट्यकला की आत्मा नहीं है, अपितु सहायक अंग है।
4. त्रासदी के उद्देश्य: करुणा और भय के माध्यम से कैथार्सिस
अरस्तु ने त्रासदी के उद्देश्य को “कैथार्सिस” (Catharsis) कहा है। यह शब्द यूनानी चिकित्सा शब्दावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है – शुद्धि, शमन या परिष्कार।
जब दर्शक नायक की पीड़ा को देखकर करुणा और भय अनुभव करते हैं, तो अंततः वे अपने भीतर की इन भावनाओं को शुद्ध कर लेते हैं। त्रासदी नकारात्मक नहीं, बल्कि मानसिक परिष्कार की ओर अग्रसर करती है। यह दर्शकों को आत्म-चिंतन और नैतिक जागरूकता की ओर ले जाती है।
5. त्रासदी का नायक
अरस्तु ने त्रासदी के नायक के लिए कुछ विशेष गुण बताए हैं:
-
नायक उच्च कुल या प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए – जिससे उसकी पतनगाथा अधिक प्रभावशाली बन सके।
-
उसमें त्रुटि (Hamartia) होनी चाहिए – जैसे अत्यधिक गर्व (Hubris), गलत निर्णय आदि।
-
उसकी नियति में पतन हो, परंतु यह केवल दैविक नहीं बल्कि उसकी त्रुटियों से हो।
-
उसके चरित्र में नैतिक द्वंद्व, संघर्ष और मानवता होनी चाहिए, जिससे दर्शक उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें।
उदाहरण स्वरूप, ओइडिपस (Oedipus) अरस्तु की त्रासदी के आदर्श नायक माने जाते हैं।
6. अरस्तु की त्रासदी अवधारणा की विशेषताएं
-
यह तर्कसंगत, संरचित और वैज्ञानिक विवेचन है।
-
यह नैतिकता और मानव स्वभाव पर आधारित है।
-
यह भावनात्मक उद्दीपन के बाद मानसिक परिष्कार की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
-
यह कलात्मक सौंदर्य और जीवन की यथार्थता का सामंजस्य प्रस्तुत करता है।
7. समकालीन दृष्टि से अरस्तु का मूल्यांकन
हालांकि अरस्तु की त्रासदी अवधारणा प्राचीन यूनानी नाटकों पर आधारित है, फिर भी इसकी सार्वकालिकता और व्यापकता इसे आज भी प्रासंगिक बनाती है।
शेक्सपीयर, कालिदास, भारतेन्दु, मोहन राकेश, गिरिश कर्नाड जैसे नाटककारों की रचनाओं में भी अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत की गूंज सुनाई देती है।
हाल के साहित्यिक विमर्शों में त्रासदी के सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों पर ध्यान दिया गया है, परंतु अरस्तु की मूल दृष्टि – ‘त्रासदी के नैतिक और भावनात्मक प्रभाव’ – आज भी आलोचकों और कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है।
उपसंहार
अरस्तु का त्रासदी विवेचन विश्व साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने त्रासदी को केवल एक भावनात्मक या करुणाजनक कथा न मानकर उसे एक सुव्यवस्थित, कलात्मक और नैतिक अनुशासन माना। त्रासदी जीवन के संघर्ष, द्वंद्व और त्रुटियों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है, जिससे वे न केवल भावनात्मक रूप से आंदोलित होते हैं, बल्कि आत्मविश्लेषण और नैतिक जागरूकता की ओर भी अग्रसर होते हैं।
आज के तकनीकी और उत्तर-आधुनिक युग में भी जब हम त्रासदी को नए संदर्भों में समझने की कोशिश करते हैं, तब भी अरस्तु की अवधारणाएं हमारी बौद्धिक और कलात्मक दृष्टि को दिशा प्रदान करती हैं। कालजयीता और सार्वभौमिकता उनके त्रासदी सिद्धांत की विशेषताएं हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
1➤ त्रासदी का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था?
2➤ अरस्तु ने त्रासदी का विवेचन किस ग्रंथ में किया है?
3➤ अरस्तु के अनुसार त्रासदी का उद्देश्य क्या है?
4➤ अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग बताए हैं?
5➤ ‘कैथार्सिस’ शब्द का अर्थ है –
6➤ अरस्तु के अनुसार त्रासदी की भाषा कैसी होनी चाहिए?
7➤ त्रासदी नायक के पतन का कारण मुख्यतः क्या होता है?
8➤ अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत का प्रभाव किस महान नाटककार पर पड़ा?
9➤ त्रासदी में ‘शुद्धि’ का तात्पर्य है –
10➤ अरस्तु ने त्रासदी के किस अंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है?